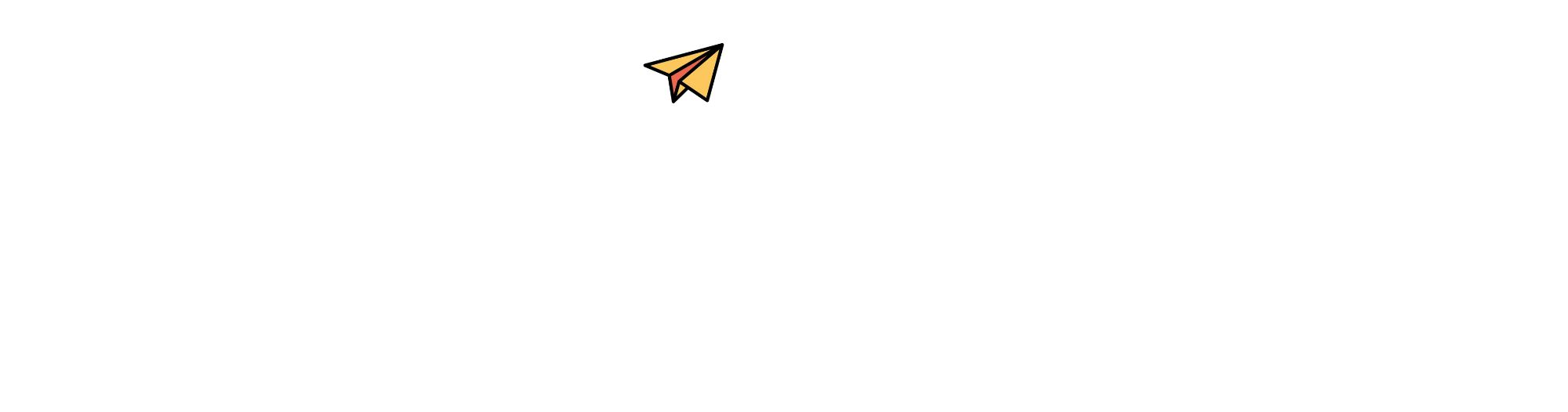भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के अंतरराष्ट्रीय उत्सव के रूप में इस बार का मातृभाषा-दिवस यूनेस्को के आयोजन का रजत जयंती वर्ष है। इसके पीछे टिकाऊ समाज के निर्माण के लिए विभिन्न भाषाओं के संरक्षण, सहनशीलता और पारस्परिक आदर का संकल्प लिया गया है। अपनी और दूसरों की भाषा को समझना अपनी और दूसरों की संस्कृति को जानने-समझने का मुख्य माध्यम है। भाषा न रहे तो हम अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ठीक से पहुँचाने में चूक जाएँगे। ऐसे में आज विश्व में प्रचलित विभिन्न भाषाओं को सुरक्षित और संवर्धित करना हमारा विशेष दायित्व है।
आशा की जाती है कि मातृभाषाओं का समादर समावेशिकता को बढ़ाएगा। एक विरल नैसर्गिक शक्ति के रूप में भाषा हमें न केवल ज्ञान-सृजन का अवसर देती है बल्कि उस ज्ञान को संजोने और दूसरों से साझा करना भी संभव बनाती है। प्रकृति भी इसे समर्थन देती है। जन्म के समय से ही हर सामान्य बच्चा भाषा अर्जित करने के उपकरण से सज्जित रहता है। नवजात की श्रवण शक्ति अद्भुत होती है। वह स्वाभाविक ध्वनि और शोर में फ़र्क़ करने लगता है। छह माह होने के पहले ही वे कई भाषाएँ सुनते और समझते रहते हैं। तीन वर्ष की आयु में उनका तीन-चार भाषाओं से परिचय स्वाभाविक रूप से होता है। दस वर्ष तक यह प्रक्रिया काफ़ी तेजी से चलती है। भारत के बच्चे स्वाभाविक रूप से बहुभाषिक परिवेश में जन्म लेते हैं और उनकी परवरिश होती है।
सांस्कृतिक स्तर पर भाषा-विकास हमारे लिए अद्भुत अवसर बन जाता है। उसी के सहारे ही हम व्यवहार करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं और उस कल्पना को मूर्त आकार भी देते हैं। लिखित रूप में आने के पहले सभी भाषाएँ वाचिक रूप में ही प्रयुक्त होती थीं । भारत में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे इस जीवन-दर्शन का एक बड़ा हिस्सा मौखिक रूप से प्राप्त होता रहा है। वेद ‘श्रुति’ के नाम से विख्यात हैं। अनुमानतः 2300 ईसा पूर्व लिखित रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया। बाद में, विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक विकास ने भाषा, संस्कृति और कलात्मक रूपों के मामले में इस क्षेत्र को अनोखी रंगत दी। इस प्रकार विभिन्न समूहों के बीच संपर्क और उनके भाषाई और सांस्कृतिक आवाजाही ने इस क्षेत्र में बहुभाषिकता के ख़ास पैटर्न को जन्म दिया। इस स्थिति ने भाषाओं में एकता आई तथा जिसने सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों को एक सूत्र में पिरोया। एकता में इस विविधता ने भारतीय सांस्कृतिक जीवन को इंद्रधनुषी रूप दिया जिसमें एक ख़ास क़िस्म का समग्रता बोध है। भारतीय भाषाओं में दृष्टिगत समानता हजारों वर्षों के सघन सांस्कृतिक संपर्क के कारण आई। धर्म, दर्शन, संगीत, भोजन, आदि सब में यह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है।
भारत सदियों से एक बहुभाषी देश के रूप में आगे बढ़ा है। यहाँ समाज का हर वर्ग, हर क्षेत्र, भाषा, कला-रूप और शैलियाँ, एक बहुरूपदर्शी (कैलिडोस्कोप) के टुकड़ों जैसे हैं। यह अनगिनत धागों की एक जटिल बुनाई की याद दिलाती है जिनमें से हर धागा जीवन के आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। परंपराओं और आधुनिक विकास ने भी इसकी बहुमुखी एकता में निरंतर योगदान दिया है। इसका जीता जागता ताज़ा प्रमाण देश के सभी भागों से आए स्नानार्थियों ने संगम तट पर दिया है। महाकुंभ के अवसर पर प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर जुटे कोटि-कोटि भारतीयों को देख कर उनकी अंतरंग सांस्कृतिक एकता और ऊपर की विविधवर्णी छवि के बीच अनोखे सामंजस्य का भाव मूर्त हो उठा। इससे यह सच प्रकट हुआ कि भारतीय समाज हमारे सामने सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई और धार्मिक प्रथाओं का एक समग्र दृश्य रचता है।
आज भारत में लगभग आठ सौ भाषाएँ दर्ज हैं। बहुतेरे भारतीय कई भाषाएँ बोलते हैं। यह बहुभाषिकता विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच न केवल संचार को प्रभावी बनाती है बल्कि साझा पहचान को सबल करती है। बावजूद इसके कि विभिन्न भाषाएँ अलग-अलग लिपियों का उपयोग करती हैं, इनमें से कई लिपियाँ एक ही मूल की हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि। यह साझा भाषाई विरासत, धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में संस्कृत भाषा और साहित्य के व्यापक उपयोग के साथ-साथ भारतीय भाषाई क्षेत्र में गहन निरंतरता विकसित करने में योगदान करती है। साझा विषय, पारस्परिक प्रभाव और समान ऐतिहासिक अनुभव इन विविध साहित्यिक परंपराओं को एक साथ बांधते हैं। तमिल–काशी संगम जैसा मेल-मिलाप संवाद के द्वारा भारतीय साहित्य एकता में विविधता की अवधारणा का प्रबल उदाहरण प्रस्तुत करता है।
भाषाओं की बहुलता समृद्धि का स्रोत है जो हज़ारों वर्षों के प्रवास, परस्पर क्रिया और विभिन्न समूहों के बीच एकीकरण से पली- बढ़ी है। भाषिक विविधता की दृष्टि से भारत आज विश्व में दूसरे नम्बर पर है। भारत के संविधान की वर्तमान व्यवस्था में 22 मुख्य भाषाएँ तथा 6 क्लासिकल भाषाएँ (तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया) सम्मिलित हैं। देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी आधिकारिक रूप से राजभाषा है हालाँकि इसके भी लगभग पचास रूप हैं। संविधान में यह विशेष प्रावधान है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकेंगे। इन सबके बीच हमें यह भी स्मरण करना होगा कि मातृभाषा अस्मिता और संस्कृति को गढ़ने का कार्य करती है। इसी दृष्टि से नई शिक्षा नीति में बहुभाषिकता, लुप्तप्राय भाषाओं का संरक्षण और स्थानीय भाषा में समावेशी शिक्षा जैसे सरोकारों पर ख़ास ज़ोर दिया जा रहा है। औपनिवेशिक विरासत के तहत अंग्रेज़ी के वर्चस्व का सामाजिक जीवन पर विभाजनकारी असर रहा है। साथ ही इसने भाषाई हीनता को भी जन्म दिया। हिंदी या अन्य भारतीय भाषा जब घर की भाषा हो तब शिक्षा में अंग्रेज़ी माध्यम कई जटिलताएँ पैदा करता है। मौलिक सोच और सर्जनात्मकता में ऐसे विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं। शोध और अनुसंधान की दृष्टि से यह परोपजीवी भाषाई संस्कार घातक सिद्ध हो रहा है।
आज भाषा की दुनिया में हो रही क्रांति में कृत्रिम बुद्धि एक महत्वपूर्ण घटक साबित हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्वीकरण तथा कृत्रिम बुद्धि की बढ़त से सभ्यताओं के अस्तित्व की चुनौती उभर रही हैं। भविष्य का नज़रिया कुछ ऐसा होने जा रहा है लोग विभिन्न गैजेट की सहायता से वह सब कुछ देखेंगे, सुनेंगे और बात करेंगे जो वैश्विक केंद्र द्वारा मुहैया कराया जाएगा। कुछ सलाह की ज़रूरत हुई तो बच्चे अब माता-पिता की जगह एलेक्सा या सीरी से पूछेंगे। उनकी माँ भी रोबोट से पूछेगी। भाषा और संचार की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में माइक्रोसाफ्ट और गूगल जैसे कई दिग्गज किरदार दुनिया की विविधता को मिटाते जा रहे हैं। इस तरह की पहल के चलते बच्चे की सर्जनात्मक क्षमता, अध्यापकों की श्रेष्ठता आदि सब दांव पर है। इस मनुष्यताविहीन तकनीक में कोई सामान्य बुद्धि या कॉमनसेंस नहीं होता। उसे मानवीय भावनाओं की भी कोई समझ नहीं होती न ग़लतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। वस्तुतः उसमें कोई अपवाद संभव ही नहीं होता। मनुष्य की तरह यह सचेतन और संवेदनशील भी नहीं है। इस तकनीक को बहुलता की कोई समझ भी नहीं होती। साथ ही उसमें घटनाओं और परिस्थितियों के संदर्भ को ग्रहण करने सुविधा नहीं होती। वस्तुतः कृत्रिम बुद्धि मानव सभ्यता की अगली गुत्थी बन रही है।
यह भरोसा किया जा रहा है कि सारा का सारा ज्ञान मानव मस्तिष्क के बाहर डाटा के रूप में भंडारित किया जा सकता है। ऐसे में प्रश्न उठेगा कि मनुष्य की ज़रूरत ही क्या है? मनुष्य को विस्थापित कर जीवन का अर्थ पाना असंभव है। ग़नीमत है मानव मस्तिष्क स्वयं को खुद संचालित और नियमित करता है। इस तकनीक को धारण करने वाले मनुष्य को मनुष्य बना रहना होगा और ऐसा करने में भाषा-साहित्य की इसमें अहम भूमिका होगी। नई शिक्षा नीति ने बहुभाषिकता की ओर ध्यान दिया है और आधारभूत भाषा तथा गणित के कौशल के विकास पर आरंभिक वर्षों में ख़ासतौर पर ज़ोर दिया जा रहा है। एक दुविधा की स्थिति यह ज़रूर है कि ऑनलाइन/डिजिटल और इंटरनेट का कितना और कब उपयोग हो। आठ वर्ष की आयु के नीचे के बच्चों के लिए इंटरनेट की सहायता से शिक्षा में हस्तक्षेप ठीक नहीं प्रतीत होती है। बच्चे तो नैसर्गिक रूप से भाषाविद् होते हैं। वे अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं की तरह कई भाषाएँ सरलता से आत्मसात् कर सकते हैं, अगर उनको बिना किसी दबाव के आसानी से सीखने का अवसर मिले। साथ ही भाषा सिर्फ़ विचारों को प्रकट करने का तरीक़ा भर नहीं होती है। वह संस्कृति का संवहन करती है। बच्चे की मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाएँ स्थानीय अर्थ व्यवस्था का आधार होती हैं। अत: स्कूली व्यवस्था को भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण में विकसित किया जाना चाहिए।
इक्कीसवीं सदी के भारत में बहु भाषिकता एक विशिष्टता है। बहुभाषिक शिक्षा अल्पसंख्यक वर्गों और आदिवासियों के लिए ख़ासतौर पर लाभप्रद होगी। आज आवश्यकता है कि फ़ौरी राजनैतिक हित-अहित को किनारे रख कर भारत के भविष्य को सुरक्षित करते हुए संतुलित भाषा नीति का कार्यान्वयन किया जाए। भाषा हमारे अस्तित्व का साधन भी है और साध्य भी।