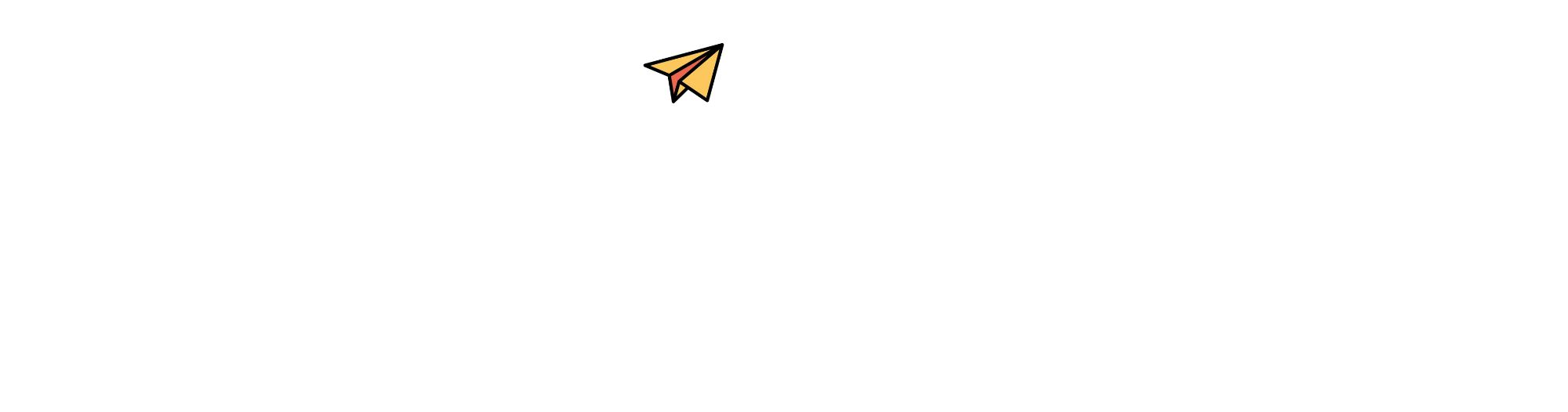स्वामी विवेकानंद ने गुरु रामकृष्ण परमहंस से एक बार पूछा, ‘आपने ईश्वर को देखा है?’ परमहंस ने जवाब दिया, ‘हाँ, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है, जैसे वे दूसरों को देखते हैं, बल्कि और भी स्पष्ट रूप से।’ ऐसे थे गुरु रामकृष्ण परमहंस। उनका जन्म 18 फरवरी, 1836 को बंगाल के कामारपुर में हुआ था। माना जाता है कि उनके दिए हुए ज्ञान का ही स्वामी विवेकानंद ने विश्व भर में प्रचार-प्रसार किया था। परमहंस 23 साल की आयु में कोलकाता के रानी रासमणि मंदिर के पुरोहित पद पर आसीन हुए थे। वे जीवनभर माँ काली की पूजा-अर्चना में संलग्न रहे।
मंदिर की सेवा में लीन, वे सादा जीवन, उच्च विचार रखते थे। उनका मानना था कि जब ईश्वर की कृपा हो जाए, तो दुनिया के दुख-दर्द नहीं रहते हैं। यदि हम ईश्वर से मिली हुई शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, तो वह वापस अपनी शक्तियाँ छीन लेगा। पुरुषार्थ से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है।
एक बार वे अपने परम भक्त मधुरदास विश्वास के साथ वृंदावन, वाराणसी और काशी विश्वेश्वर की यात्रा पर रेल से निकले। यात्रा के दौरान बिहार के वर्धमान गाँव में रुके। उस समय बिहार अकाल की भयंकर चपेट में था। अन्न और जल दोनों की कमी थी। जनता दुख और कष्टों से बेहाल थी। करुणामय रामकृष्ण परमहंस यह स्थिति देखकर व्यथित हो गए। उन्होंने अपने साथी मधुरदास से कहा, “देखो, भारत माँ की संतानें कैसी दीन और हीन भाव से ग्रस्त हैं। आप इन दरिद्रनारायण के भरपेट भोजन की व्यवस्था करो, तभी मैं यहाँ से आगे जाऊँगा। मैं इन्हें तड़पते-बिलखते नहीं छोड़ सकता।” यह कहने के साथ ही उनकी आँखों से आँसू बहने लगे। मधुरदास कोलकाता गए और उनके लिए भोजन व राशन की व्यवस्था की। उनके इस असीम प्रेम से उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। इसके बाद ही परमहंस ने आगे की यात्रा पूरी की।
एक बार रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों से कहा कि ईश्वर एक है, उस तक पहुँचने के मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है – ईश्वर तक पहुँचना। भक्ति के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। यह सुनकर एक शिष्य ने कहा, “हम यह कैसे मान लें कि सभी रास्ते सत्य हैं?” इस पर उन्होंने शिष्य को समझाते हुए कहा, “किसी अनजाने घर की छत पर पहुँचना कठिन है। छत पर पहुँचने के लिए हम सीढ़ी, रस्सी या बांस का सहारा लेंगे। छत पर पहुँचने के बाद हमें पता चलेगा कि हम सबका लक्ष्य एक ही था, लेकिन पहुँचने के तरीके अलग-अलग थे। हमें भक्ति करते समय किसी एक मार्ग को दृढ़तापूर्वक अपनाना चाहिए और अलग-अलग रास्ते देखकर भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अंतिम लक्ष्य एक ही है।”
परमहंस विवेकानंद को समझाया करते थे कि समाज की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चारों ओर भूख, रोग, अशिक्षा और अज्ञानता फैली हुई है। हिमालय में तपस्या करने से बेहतर है कि वे इन समस्याओं से जूझ रहे लोगों की मदद करें। स्वामी विवेकानंद ने कठोर तपस्या करने के स्थान पर समाज की सेवा को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया।
रामकृष्ण परमहंस का गुरु के बारे में मानना था कि संत बुरे व्यक्तियों में भी उनके अंदर की अच्छाइयों को ढूँढ़ निकालते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से बैर न रखे और हर चीज में अच्छाइयों को खोजे। अहंकार ही असली रूप में माया है। इस अहंकार को त्याग देना चाहिए। अहंकार को त्यागकर ही मानव अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है।
उनका कहना था कि मानव को निःस्वार्थ भाव से सेवा और मदद करनी चाहिए, भले ही सामने वाला उसका साथ दे या न दे। वे उदाहरण देकर समझाते थे कि यदि हम नदी में गोता लगाते हैं और हमें पहली बार में मोती नहीं मिलता, तो इसका मतलब यह नहीं कि समुद्र में मोती नहीं हैं। वे यह बताना चाहते थे कि मनुष्य को जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। भले ही पहली बार में सफलता हाथ न लगे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सफलता मिलेगी ही नहीं।
परमहंस कहा करते थे, “व्यक्ति का मन ही उसे गुलाम, बादशाह, ज्ञानी और अज्ञानी बनाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करके अपना मार्ग सुगम बनाना चाहिए।” वे कहा करते थे कि व्यक्ति देखने में अलग-अलग हो सकते हैं – कोई गोरा, कोई काला, कोई क्रूर। लेकिन सभी में ईश्वर का तत्व मौजूद है। इसलिए सभी में ईश्वर की छवि देखनी चाहिए।
मनुष्य को अपने जीवन में त्याग की भावना रखकर यापन करना चाहिए। उनका कहना था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। व्यक्ति को इस सच्चाई को पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा उसे अपनी चीजें खोने का दर्द हमेशा सताता रहेगा।
गुरु रामकृष्ण का आदर्श वाक्य है – ‘शिव ज्ञाने जीव सेव’, जिसका अर्थ है कि ‘मनुष्य की सेवा ही भगवान की पूजा है।’