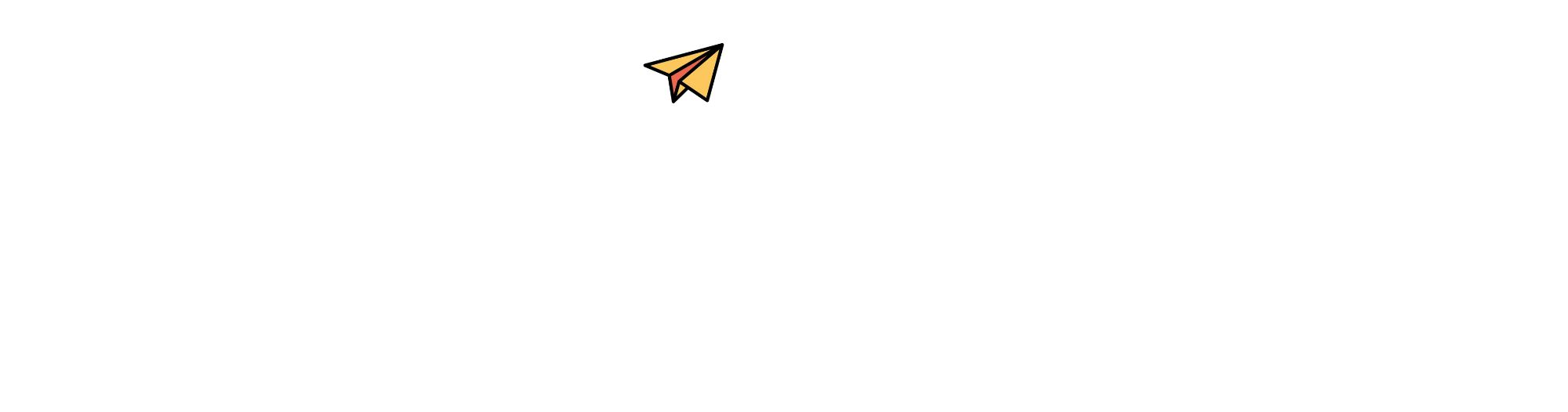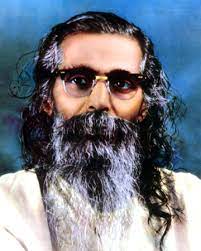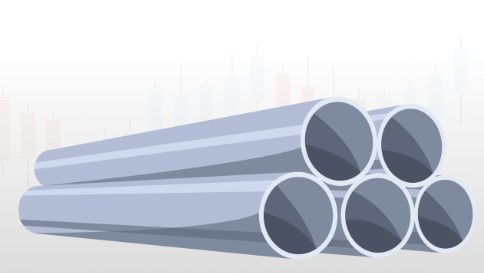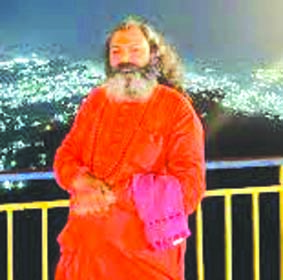राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें सभी लोग गुरुजी के नाम से पुकारते हैं, उनका दर्शन और विश्वदृष्टि, सनातन धर्म के ठोस और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी, जिससे उनका दृष्टिकोण स्पष्ट और असंदिग्ध था। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके विचार प्राचीन सिद्धांतों से अडिग रूप से बंधे हुए थे। सेमेटिक धर्मों के विपरीत, हिंदू धर्म ने लगातार लचीलापन और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन किया है। सनातन धर्म मौलिक और शाश्वत है, फिर भी हमारे ऋषियों ने समय के निरंतर बीतने के कारण परिवर्तन की अनिवार्यता को पहचाना। नतीजतन, सनातन धर्म के सिद्धांतों को आँख मूंदकर या कट्टरता से नहीं बल्कि सोच-समझकर और प्रासंगिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। गुरुजी ने इस अंतर को अच्छी तरह से समझा और तदनुसार मार्गदर्शन प्रदान किया।
जीवों में एक सुखी, देखभाल करने वाला और शांतिपूर्ण जीवन जीने की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है। हालाँकि, जैसे-जैसे दुनिया ने पश्चिमीकरण को अपनाया है, विकसित भौतिकवादी मानसिकता ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर भारी असर डाला है, जिससे वे अपने आसपास की शांति, आनंद और सामंजस्य खो रहे हैं। अधिकांश लोग लालच, शत्रुता, विनाशकारी मानसिकता और अहंकारी रवैये जैसी कई नकारात्मक विशेषताओं के साथ एक यांत्रिक अस्तित्व जीते हैं, मानवता की भावना को खो रहे हैं और प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और उच्च जीवन स्तर के बावजूद, दुनिया भर के व्यक्ति दुखी, असंतुष्ट हैं और सामाजिक अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। पश्चिमी उपभोक्तावाद की अवधारणा हानिकारक है, क्योंकि यह व्यक्तियों को केवल वस्तुओं और ग्राहकों के रूप में देखता है। इससे सभी उपलब्ध रास्तों का शोषण होता है, अक्सर मानवता और पर्यावरण अखंडता की कीमत पर। इसके अलावा, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सामाजिक संबंध और कल्याण को बढ़ावा देने के बजाय उपभोक्तावाद पर ध्यान केंद्रित करके डिज़ाइन किया गया है। इसलिए गुरुजी की शिक्षाएँ आज की दुनिया में अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्हें समाज, राष्ट्र और विश्व के सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक आयामों की पूरी जानकारी है। उनकी कुछ शिक्षाएँ हमारी बेहतर समझ के लिए प्रस्तुत हैं।
गुरुजी के आर्थिक, राजनीतिक और स्वदेशी सिद्धांत
किसी समाज की राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पूर्ण समाज पर भी पड़ सकता है। गुरुजी ने एक एकीकृत सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक दृष्टिकोण विकसित किया। उन्होंने भारतीय दर्शन, संस्कृति, धर्म और साहित्य के साथ-साथ समाजवाद, मार्क्सवाद और पश्चिमीकरण जैसी पश्चिमी विचारधाराओं का भी गहन अध्ययन किया। अपने व्याख्यानों और भाषणों में उन्होंने मार्क्सवाद और पश्चिमीकरण दोनों की आलोचना की। वे अक्सर भारतीय दर्शन और साहित्य की तुलना मार्क्सवाद और उसकी विचारधारा से करते थे। गुरुजी ने मार्क्सवाद के आर्थिक नियतिवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के मूल सिद्धांतों को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि न तो साम्यवाद और न ही पूंजीवाद दुनिया को एकजुट कर सकता है। उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया वह आवश्यक था। भौतिकवादी विचारधारा, जो मनुष्यों को भौतिक पशु मानती है और भौतिक हितों को प्राथमिकता देती है, एकता और सद्भाव के बजाय प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को जन्म देती है। तर्क सीधा है। भौतिक स्तर पर, केवल विविधता और अंतर है। वे अलगाववाद और बहिष्कार को बढ़ावा देते हैं। जो व्यक्ति केवल भौतिक वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनमें एकता और एकीकरण की कमी हो सकती है। सहयोग पर विचार करने का कोई कारण नहीं है। जब हम स्पष्ट मतभेदों से परे देखते हैं, तो हम एक सूक्ष्म एकता देख सकते हैं जो सभी स्थूल प्राणियों को एक सुसंगत पूल में जोड़ती है।
गुरुजी के अनुसार, भौतिकवादी मानते हैं कि हम सभी स्वतंत्र व्यक्ति हैं जिनका कोई सामान्य संबंध या लगाव नहीं है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद पर वर्गहीन समाज की जीत पर केंद्रित हैं। उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया कि आपसी नापसंदगी और दुश्मनी सफलता की ओर ले जा सकती है। उन्हें लगा कि साम्यवाद वर्ग विभाजन और नफरत पैदा कर सकता है, जो अंततः वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा कटुता और आपसी दुश्मनी पर जोर देती है। उन्होंने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए वर्ग शांति, सहयोग और आपसी समझ पर जोर दिया। उनका मानना था कि वर्ग भेद समाज को विभाजित करते हैं, जो राष्ट्र के लिए हानिकारक है। सोवियत संघ और चीन को व्यापक रूप से मार्क्सवादी-आधारित साम्यवाद के सबसे प्रमुख उदाहरण माना जाता है। उनके अनुसार, चीन और रूस ने ऐतिहासिक रूप से सत्ता हासिल करने के लिए समाजवाद का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण विनाशकारी कदम उठाए गए हैं। दोनों देशों में प्रभुत्व के भूखे अधिकारियों ने राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए ऐतिहासिक रूप से अपने ही नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है। चीन और रूस उन्नत और विकसित होने का दावा करते हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य वैश्विक प्रभुत्व स्थापित करना है। गुरुजी इस स्वभाव और व्यवहार को राक्षसी मानते हैं।
उपभोक्तावाद हिंदू संस्कृति के लोकाचार के साथ असंगत है। हमारा आदर्श वाक्य “अधिकतम उत्पादन और समान वितरण” होना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता हमारा तात्कालिक लक्ष्य हो। बेरोजगारी और अल्परोजगार को युद्ध स्तर पर संबोधित किया जाना चाहिए। जबकि औद्योगीकरण आवश्यक है, लेकिन इसे पश्चिम की नासमझ प्रतिकृति होने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति का दोहन किया जाना चाहिए, शोषण नहीं। पारिस्थितिकी कारक, प्राकृतिक संतुलन और भावी पीढ़ियों की जरूरतों पर विचार किया जाना चाहिए। पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्र और नैतिकता सभी पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक नव स्वतंत्र राष्ट्र के नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने नागरिकों की मानसिक संरचना में आवश्यक परिवर्तन को प्रभावित करना है। गुरुजी नव स्वतंत्र भारत की मानसिकता से अच्छी तरह वाकिफ थे। अंग्रेजों ने भारत को न केवल राजनीतिक और आर्थिक रूप से गुलाम बनाया था, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में सांस्कृतिक रूप से भी गुलाम बनाया था। वे अपनी दुर्भावनापूर्ण योजनाओं में काफी हद तक सफल भी हुए थे।
हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने इस सत्य को समझा और स्वदेशी, गोरक्षा, स्वभाषा, हिंदी आदि पर जोर देकर इस आत्मघाती मानसिकता को खत्म करने का प्रयास किया। डॉक्टर जी का अनुसरण करते हुए गुरुजी ने संघ के माध्यम से लोगों में इन विचारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहल की। स्वदेशी पर उनका विश्वास सर्वव्यापी था। स्वदेशी की उनकी अवधारणा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तक सीमित नहीं थी; इसमें दैनिक जीवन के सभी तत्व शामिल थे, जैसे कि हमारी मूल भाषाओं में विवाह के निमंत्रण या कार्यक्रम की बधाई भेजना, साथ ही हिंदू परंपरा के अनुसार जन्मदिन मनाना आदि।
इन दृष्टिकोणों का विशेष महत्व है। ये केवल दार्शनिक ग्रंथ नहीं हैं। गुरुजी केवल एक बौद्धिक दार्शनिक से कहीं अधिक थे। वे हिंदू दर्शन और उसकी जटिलताओं को अच्छी तरह समझते थे। एक व्यावहारिक नेता और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपने दर्शन को व्यक्तिगत अनुभव और प्रयोग के माध्यम से परखा। वे वास्तविक दुनिया के मुद्दों और चुनौतियों पर केंद्रित रहे। उनका दृष्टिकोण हिंदू आध्यात्मिक परंपरा पर आधारित होने के बावजूद अत्यधिक व्यावहारिक था।